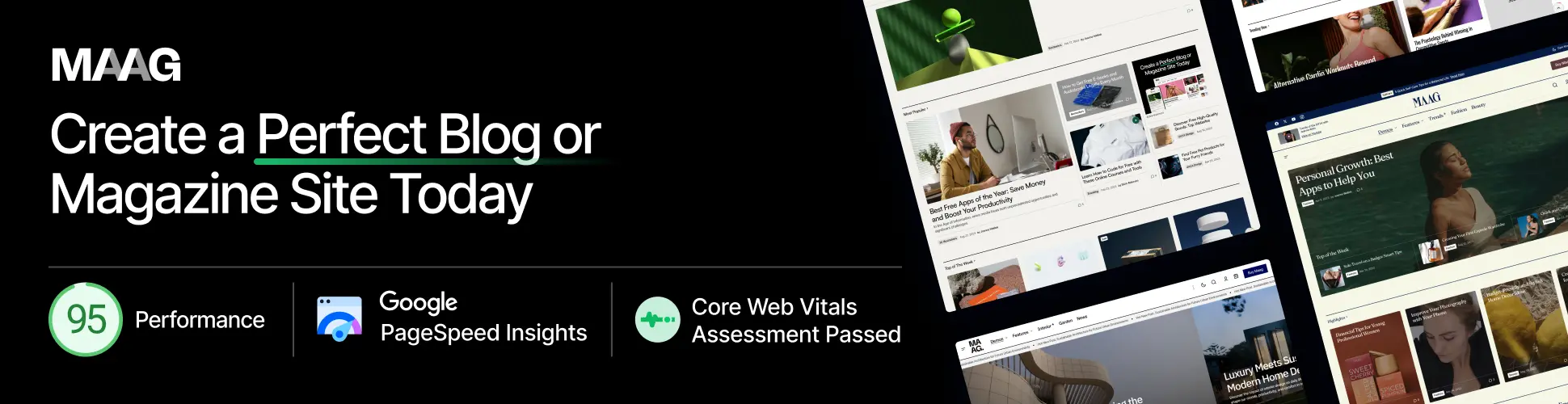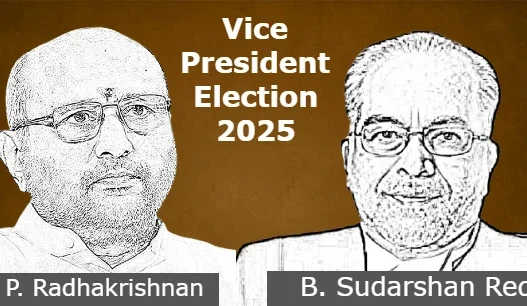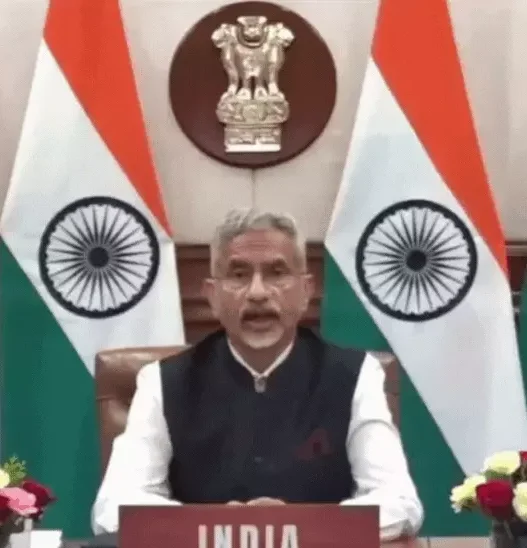भारत में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि इनमें मानवीय गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव है।
लगातार बारिश और बादल फटने से उत्तरी हिमालय में तबाही मची है, उत्तराखंड में पाँच लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हैं। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से गाँव तबाह हो गए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी ने राजमार्गों और घरों को निगल लिया है, जबकि बर्फ से भरी नदियों ने पंजाब के खेतों को जलमग्न कर दिया है।
पहाड़ी घाटियों से लेकर मैदानी इलाकों तक , समुदाय फंसे हुए हैं, बचाव अभियान समय के साथ दौड़ रहे हैं, और परिदृश्य बदल गए हैं। पड़ोसी पाकिस्तान और चीन में भी स्थिति अलग नहीं है।
भारत में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ें कोई अकेली प्राकृतिक आपदा नहीं हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित शहरीकरण, अति-पर्यटन और नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव जैसी मानवीय गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव है।
ह घातक संयोजन तेजी से चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, तथा देश भर में बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहा है, क्योंकि मौसम की मार पड़ रही है।
हिमालय, जिसे “तीसरा ध्रुव” कहा जाता है, विशेष रूप से असुरक्षित है। वहाँ के ग्लेशियर और पर्माफ्रॉस्ट दस प्रमुख एशियाई नदियों को पोषण देते हैं जो 1.3 अरब से ज़्यादा लोगों का जीवन यापन करती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने उनके पीछे हटने की गति तेज़ कर दी है, जिससे पानी का प्रवाह अप्रत्याशित हो रहा है और बाढ़, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
इस क्षेत्र में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से अधिक हो गई है, अनियमित, तीव्र मानसूनी वर्षा लगातार हो रही है, जिससे हिमालय की नाजुकता और बढ़ गई है।
अनियंत्रित शहरीकरण इस संकट को और बढ़ा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई भारतीय शहरों में तेज़, अनियोजित विकास हुआ है, जिसके कारण प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों का कंक्रीटीकरण हुआ है, आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण हुआ है, और उन झीलों का क्षरण हुआ है जो कभी बाढ़ के पानी के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक का काम करती थीं।

पुराना जल निकासी ढांचा, अपशिष्ट प्रबंधन के कुप्रबंधन से अवरुद्ध जलमार्ग, और अभेद्य सतहें भूमि की वर्षा अवशोषण क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे भारी वर्षा शहरी बाढ़ में बदल जाती है जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और भारी आर्थिक क्षति होती है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु की 80% से अधिक झीलों के नष्ट हो जाने से बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन तनाव का एक और स्तर बढ़ा देता है। तीर्थयात्रा और पर्यटन सुविधाओं के लिए अनियंत्रित निर्माण कार्य नाज़ुक पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर देता है, जिससे भूस्खलन और कटाव का खतरा बढ़ जाता है। सड़कों, जलविद्युत और खनन के लिए वनों का विनाश मिट्टी के क्षरण और अपवाह को और बढ़ा देता है, जिससे बाढ़ और भी विकराल हो जाती है।
हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में बताया गया है कि भारत, ब्राजील और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में गर्मी से संबंधित 28,000 मौतें सीधे तौर पर इन क्षेत्रों में बढ़ते वनों की कटाई के कारण हुई हैं।

जलवायु परिवर्तन एक “बल गुणक” के रूप में कार्य करता है, जो इन मानवीय गतिविधियों के प्रभावों को तीव्र करता है।
बादल फटने, बेमौसम भारी बारिश, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) और पिघलते ग्लेशियरों से जुड़ी अचानक बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति दर्शाती है कि किस तरह प्राकृतिक रूप से कमजोर क्षेत्र मानव-चालित पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं।विज्ञापन
इन परस्पर जुड़ी समस्याओं के लिए एकीकृत समाधान की आवश्यकता है, जलवायु कार्रवाई को मजबूत करना, टिकाऊ शहरी नियोजन, पुनर्वनीकरण, पर्यटन और निर्माण का सख्त विनियमन, तथा आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
तत्काल उपाय न किए जाने पर, बाढ़ की विकराल होती स्थिति इस बात की प्रारंभिक चेतावनी है कि मानव ने स्वयं ही अपनी आपदाएं उत्पन्न कर ली हैं, जिससे पूरे भारत में जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो गया है।
आज भारत में बाढ़ का प्रकोप केवल प्रकृति का कृत्य नहीं है, बल्कि यह मानवीय निर्णयों और जलवायु तथा भूदृश्यों पर उनके प्रभावों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
इसका समाधान करने के लिए हमें अपनी भूमिका को स्वीकार करना होगा तथा लोगों और ग्रह दोनों की सुरक्षा के लिए स्थिरता को अपनाना होगा।